जिस पर मुझे जरूरत से ज्यादा गुमान था
दिल उस शख्श का बहुत बेईमान था ।
बिखरा हुआ पढ़ा था एक साया उसके पास
कोई अजनबी नहीं वो मेरा अरमान था ।
कहकहों में बज्म के दब गई सिसकी मेरी
मामूली थी हस्ती मेरी , बहुत छोटा निशान था ।
खुश था जिसे फूंककर मज़हबी जूनून में
बाद में मालुम हुआ वो मेरा मकान था ।
दोस्ती भी दोस्तों ने निभाई तो किस जगह
बस जिंदगी से चार कदम दूर शमशान था ।
भूख का कोई कहीं मज़हब 'दीपक' होता नहीं
काफिर के साथ खा गया जो मुसलमान था ।
( उपरोक्त ग़ज़ल काव्य संकलन मंज़र से ली गई है )
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
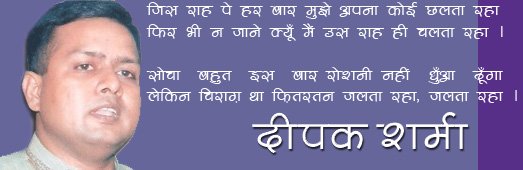
.jpg)

No comments:
Post a Comment